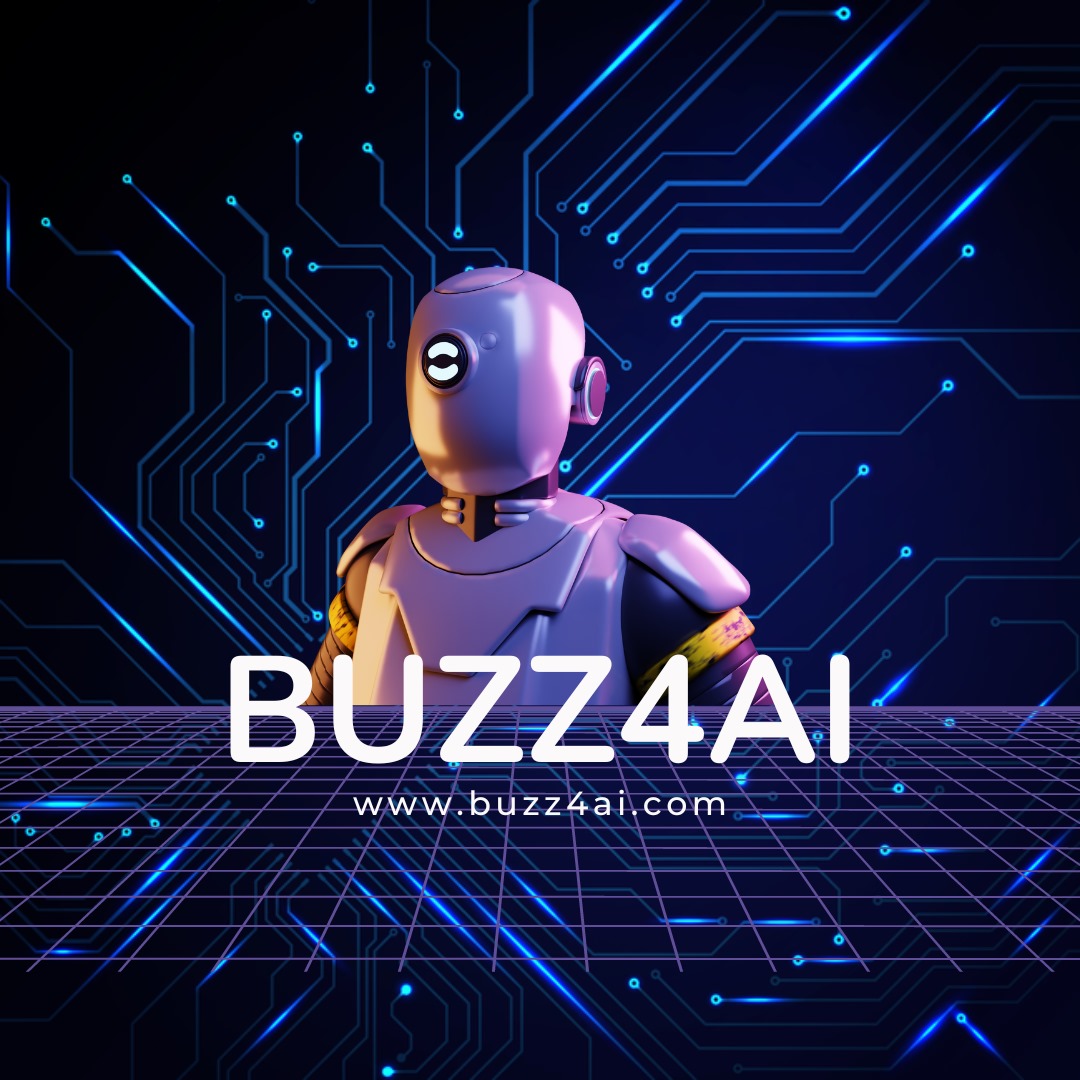भारत में नदियां केवल जल ही नहीं, अपने साथ-साथ जीवन की ही धारा सहेजे हुए हैं। भारतीय जनजीवन में इनकी पैठ इतनी गहरी है कि नदियों के बिना यहां जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन्हें स्वच्छ, पवित्र और इनके प्रवाह को निर्बाध बनाए रखना ही इनकी सच्ची पूजा होगी।
भारतीय जनजीवन में नदियों का योगदान इतना अधिक है कि इस विषय पर कितने ही ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, औषधि और न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे-सीधे जुडे हुए हैं। किसी भी अन्य सभ्यता से बहुत लंबे समय तक हमने नदियों को धर्म से जोड कर इन्हें स्वच्छ और पवित्र भी बनाए रखा। यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन आधुनिकता के साथ शुरू हुई उपभोक्तावाद की अंधी दौड और उसमें बिना सोचे-समझे सभी के कूद पडने का नतीजा यह हुआ कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को स्वयं ही नष्ट करने पर तुल गए।
सदियों से भारत में नदियों की पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू जन नदियों को भगवान के स्वरूप मानते रहे हैं। कई नदियों को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती रही है। नदियों की पूजा की यह परंपरा तो अभी भी चली आ रही है, लेकिन यह परंपरा शुरू होने के मूल में निहित भावना का लोप सा हो गया है। हमारे यहां लगभग सभी नदियों को आज भी मां के रूप में सम्मान दिया जाता है। गंगा ही नहीं, देश की दूसरी नदियों के प्रति भी हमारे मन में गहरा सम्मान है। चूंकि सम्मान का यह भाव हमें हमारी परंपरा से मिला है, इसीलिए इसे सीखने के लिए हमें किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में जाने की जरूरत नहीं होती। किसी छोटे-बडे धक्के से यह सम्मान टूटता भी नहीं। क्योंकि यह हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है।
इसी कारण से यहां माना जाता है कि गंगा में नहाने भर से इंसान शुद्ध हो जाता है। देश की दूसरी नदियों को भी हम गंगा से कम महत्वपपूर्ण नहीं मानते। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा माता को देखने भर से इंसान शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक नदी से कोई न कोई कथा जुडी हुई है। दुर्भाग्य यह रहा कि बाद के दिनों में वैज्ञानिक चेतना के नाम पर धर्म से जुडी मान्यताओं का उपहास उडाने की प्रवृत्ति पनपने लगी। इस क्रम में परंपरा के निहितार्थ को न तो तलाशने की ईमानदार कोशिश की गई और न लोगों तक उसके मूल तत्व को पहुंचाने की ही। इस तरह न तो वैज्ञानिक मान्यताओं को स्थापित किया जा सका और न कोई वैज्ञानिक चेतना ही जगाई जा सकी, हां अपनी परंपरा के उदात्त मूल्यों से लोगों को अलग जरूर कर दिया गया।
हिंदू लोग जिस तरह आसमान में सप्त ऋषि के रूप में सात तारों को पूच्य मानते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर सात नदियों को पवित्र मानते हैं। जैसे आसमान में ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि अगत्स्य, ऋषि अत्रि एवं ऋषि जमदग्नि अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं, वैसे ही पृथ्वी पर सात नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, शिप्रा एवं गोदावरी अपने भक्तों की सुख एवं समृद्धि के लिए निरंतर बहती रहती हैं। गंगा नदी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ द्वारा भगवान महादेव के तप की पौराणिक कथा पूरे देश में लोकप्रिय है।
देश में नदियों के योगदान एवं महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वाराणसी आज विश्व के प्राचीनतम नगर एवं प्राचीनतम जीवित सभ्यता के रूप में जाना जाता है और वाराणसी गंगा के तट पर बसा हुआ है। आज वाराणसी विश्व में धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक नगर के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके अलावा प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नासिक, उच्जैन, गुवाहाटी, गया, पटना आदि सभी प्रमुख प्राचीन शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, हुबली आदि आधुनिक नगर भी नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं।
इससे स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन काल से ही नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। इसी महत्व को देखते हुए यहां नदियों की पूजा की परंपरा स्थापित हुई। यह परंपरा हमारे यहां आज भी पहले की ही तरह चली आ रही है, लेकिन इसके मूल में निहित वास्तविक उद्देश्य हम भूल चुके हैं। इस परंपरा की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने नदियों को धन्यवाद ज्ञापित करने और उनके प्रति नई पीढी के मन में सम्मान का भाव बनाए रखने के लिए ही किया था। धन्यवाद ज्ञापन इसलिए, क्योंकि हमें नदियों से बहुत कुछ मिलता है। प्राचीन काल ही नहीं, आज भी बहुत हद तक हमारा जीवन नदियों पर निर्भर है। इनके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम इनकी स्वच्छता और पवित्रता को चिरकाल तक बनाए रख सकें। तभी इनका जल हमारे लिए उपयोगी हो सकेगा और हम लंबे समय तक इनका लाभ उठा सकेंगे। दुर्भाग्य से अब इस वैज्ञानिक सोच से हम भटक गए हैं और पूजा के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, वह कर्मकांड से अधिक कुछ नहीं रह गया है।
स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुए अनियोजित विकास और दिशाहीन औद्योगीकरण ने नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इससे हमें सिर्फ सामाजिक ही नहीं, आर्थिक क्षति भी उठानी पडी है। नदियों पर आधारित कृषि, पर्यटन आदि बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदियों के प्रदूषित होने के कारण भूमि भी प्रदूषण से प्रभावित होने लगी। इसका सीधा असर कृषि उपज की गुणवत्ता पर पडा। परिणामस्वरूप किसान एवं गांव के साथ-साथ सबकी सेहत पर उलटा असर पडा।
कहा जाता है कि ब्रिटिश संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब यात्रा के लिए चलते थे तो पीने के लिए गंगाजल लेकर चलते थे जो इंग्लैंड पहुंचकर भी खराब नहीं होता था तथा यात्रा के बाद बचे हुए पानी को भी फेंका नहीं जाता था। नाविक लोग अपने घर ले जाते थे तथा वह पानी पीने में उपयोग करते थे। ब्रिटिश सेना भी युद्ध के समय गंगाजल अपने साथ रखती थी जिससे कि घायल सिपाही के घाव को धोया जाता था। इससे घाव में इन्फेक्शन नहीं होता था। गंगा का जल आज भी हिंदू लोग अपने घरों में रखते हैं और कई जगहों पर हो गए प्रदूषण के बावजूद वह वर्षो तक खराब नहीं होता।
परन्तु, धीरे-धीरे लोगों ने नदियों में सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलिथीन आदि डालना शुरू कर दिया जिससे आज भारत की नदियां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं। दिल्ली में यमुना, कानपुर में गंगा, मुम्बई में मीठी नदी अत्यंत प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके नदियों का पानी ही नहीं, अपितु आसपास की भूमि भी प्रदूषित होकर बंजर होती जा रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है।
तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण ने नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को खत्म ही कर दिया है। नदियों के तटीय क्षेत्र, डूब की भूमि, वेटलैंड आज अवैध निर्माण से भर गए हैं तथा वहां की आबादी नदियों को प्रदूषित कर रही है।
इन कारणों से नदियों का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ गया है। कई नदियां तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसका सीधा असर प्राकृतिक संतुलन पर पड रहा है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें नदियों को प्रदूषणमुक्त करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले नदियों के किनारों से, नदियों के डूब के क्षेत्र से, तथा वेटलैंड से अवैध बस्तियों तथा अवैध निर्माण को हटाना होगा। जिससे नदियों को फैलने का पूरा मौका मिले।
इसके साथ ही साथ देश को नदियों के शुद्ध पानी तथा बारिश के पानी को रोकने के लिए भी हमें बडे कदम उठाने होंगे। इसके लिए नदियों को जोडा जाना एक श्रेष्ठ उपाय है। इसी के साथ नदियों पर हर पचास किलोमीटर पर बांध का निर्माण किया जाए। नदियों के तटों पर बडी संख्या में वृक्ष लगाए जाएं तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बडे पैमाने पर व्यवस्था की जाए।
इन सभी उपायों से नदियों के प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ ही साथ बाढ एवं सूखा को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। देश में पीने के पानी की कमी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है।
जहां एक ओर नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर उनमें सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलिथीन, शव आदि डाले जा रहे हैं। ऐसी पूजा का अर्थ ही क्या है? ध्यान रहे, कर्मकांड से नदी की प्रसन्नता हमें मिलने वाली नहीं है। हमें वास्तव में नदियों का सम्मान करना सीखना होगा। इसके लिए हमें स्वयं संकल्पबद्ध होना होगा और स्वयं से किया यह संकल्प हर हाल में निभाना होगा। यही उनकी सच्ची पूजा होगी। अन्यथा आने वाले समय में बाढ, सूखा, जल संकट भूमि प्रदूषण ही नहीं अपितु उत्तरांचल जैसी भयावह प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी होंगी।
डॉ. योगेश शर्मा
दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. योगेश शर्मा अंग्रेजी के कवि हैं। अंग्रेजी में डॉ. शर्मा की कई कहानियां, निबंध और शोधपत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। आध्यात्मिक अभिरुचि के साथ-साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले योगेश का इन्फ्लूएंस ऑफ भगवद्गीता ऑन मैथ्यू आर्नोल्ड विषय पर शोध रहा है। भारतीय इतिहास में भी इनकी गहरी दिलचस्पी है।
सच सदा के लिए
ज्ञान के परदे की ओट के बिना देखना अवलोकन में किसी तरह के संचित ज्ञान की जरूरत नहीं, हालांकि ज्ञान एक स्तर विशेष तक सहजत: आवश्यक है। जैसे चिकित्सीय ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, इतिहास का ज्ञान और अन्य सारी चीजों का जो हैं। क्योंकि अंतत: वे सब चीजें जो हो चुकी हैं, हैं -उनके बारे में सूचना, ज्ञान है। लेकिन भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, बस जो हो चुका है उसके ज्ञान के आधार पर लिए अंदाजे ही हमें भविष्य के साथ जोडने वाली कडी हैं। एक ऐसा मन जो ज्ञान के झीने परदे की ओट से देख रहा है, वह विचार की तीव्र धारा का अनुगमन करने में सक्षम नहीं हो सकता। यदि आप अपनी ही संपूर्ण वैचारिक संरचना को देखना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान के झीने परदे को हटाकर, अपनी संपूर्ण वैचारिक संरचना को सीधे देखना होगा।