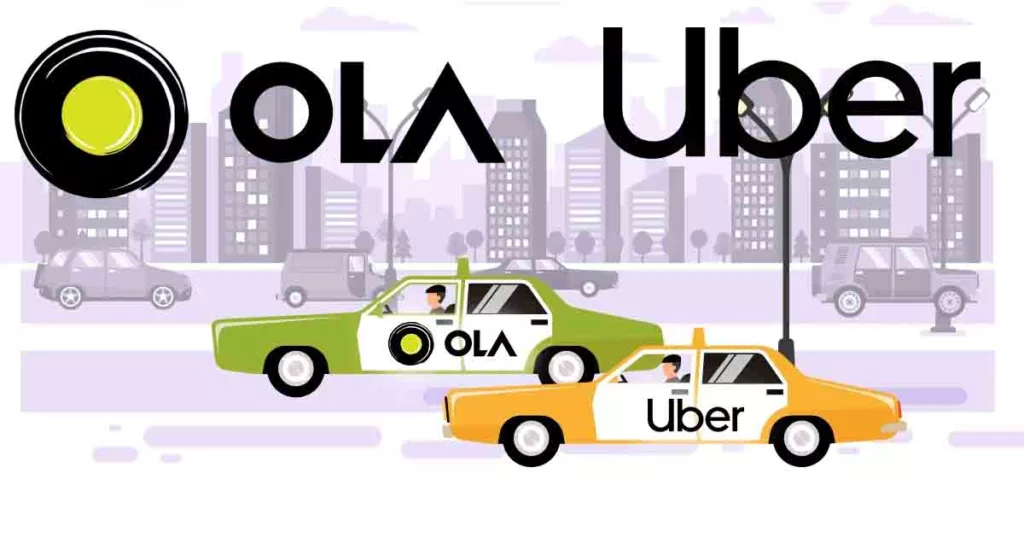ऐसी दुनिया में जहाँ मिसाइलें हज़ारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकती हैं, भारत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक अरब से ज़्यादा की आबादी और सुरक्षा के लिए ज़रूरी संपत्तियों के साथ, हमारा देश चुपचाप एक मज़बूत मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो आसमान में एक दिव्य किला है। अक्सर इज़राइल के आयरन डोम से तुलना की जाने वाली, भारत की ढाल कहीं ज़्यादा जटिल है, जिसे पाकिस्तान की सामरिक मिसाइलों से लेकर चीन के उन्नत बैलिस्टिक शस्त्रागार तक, कई तरह के ख़तरों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है और वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, क्या भारत की मिसाइल रक्षा कल के ख़तरों को मात दे सकती है? आइए सरल भारतीय अंग्रेज़ी में सुरक्षा के इस उच्च-दांव वाले खेल का पता लगाते हैं।
भारत की मिसाइल रक्षा एक बहु-स्तरीय जाल की तरह है, जो उड़ान के अलग-अलग चरणों में ख़तरों को पकड़ती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की अगुआई में इस प्रणाली ने कारगिल युद्ध के बाद 2000 के आसपास आकार लेना शुरू किया। चेतावनी स्पष्ट थी: पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी परमाणु-सक्षम मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में भारत को एक मज़बूत रक्षा की ज़रूरत थी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसे दो चरणों में विभाजित किया गया। चरण 1 में 2,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से निपटा जाता है, जो तत्काल क्षेत्रीय खतरों को संबोधित करता है। चरण 2, जो अभी भी प्रगति पर है, का उद्देश्य 5,000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की मिसाइलों और संभवतः अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) का भी मुकाबला करना है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण एक ऐसी दुनिया में आगे रहने के भारत के संकल्प को दर्शाता है जहाँ खतरे केवल चालाक होते जा रहे हैं।
इस किले के केंद्र में पृथ्वी वायु रक्षा (PAD), या प्रद्युम्न, रक्षा की पहली पंक्ति है। पृथ्वी से 50-80 किलोमीटर ऊपर, बाहरी वायुमंडल में संचालित, PAD हमारी धरती से दूर, उड़ान के दौरान मिसाइलों को बीच में ही रोक देता है। इसे मध्यम और मध्यम दूरी की मिसाइलों (अभी 3,000 किलोमीटर तक, संभावित रूप से 5,000 किलोमीटर बाद) को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। “हिट-टू-किल” पद्धति का उपयोग करते हुए, PAD आने वाली मिसाइलों पर हमला करता है, और उन्हें पूरी ताकत से नष्ट कर देता है, चाहे वे पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा रहे हों। मैक 5 की तेज गति और स्वोर्डफ़िश (जो 1,500 किमी दूर से खतरों को पहचान सकता है) जैसे लंबी दूरी के रडार द्वारा समर्थित, PAD एक उच्च तकनीक वाला रक्षक है। लेकिन क्या यह तब भी टिक पाएगा जब दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करते हैं जो अप्रत्याशित रूप से ज़िग-ज़ैग करती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देने के लिए DRDO दौड़ रहा है।
दूसरी परत, एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD), या अश्विन, घर के करीब, वायुमंडल के अंदर 15-40 किमी की ऊँचाई पर कदम रखती है। यदि PAD चूक जाता है, तो AAD को दूसरा शॉट मिलता है। यह कम दूरी की मिसाइलों (2,000 किमी तक) को निशाना बनाता है और “हिट-टू-किल” तकनीक का भी उपयोग करता है। मैक 4.5 की गति से चलते हुए, स्मार्ट रडार द्वारा निर्देशित, और मोबाइल लॉन्चर पर लगे, AAD तेज़ और लचीला है। इसकी गतिशीलता दुश्मनों के लिए इसे पहचानना कठिन बनाती है, लेकिन जैसे-जैसे मिसाइल तकनीक आगे बढ़ती है, क्या AAD की ऊंचाई और गति अगली पीढ़ी के खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त होगी? PAD और AAD का स्तरित दृष्टिकोण भारत को मिसाइल को रोकने के कई मौके देता है, लेकिन कोई भी सिस्टम फुलप्रूफ नहीं है, खासकर मिसाइलों के झुंड या रडार को भ्रमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नकली मिसाइलों के खिलाफ। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा, भारत को लड़ाकू जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। आकाश मिसाइल प्रणाली में प्रवेश करें, जिसका अर्थ है “आकाश।” आकाश एक स्थानीय प्रहरी की तरह है, जो हवाई हमलों से प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा करता है। 25-45 किमी (और इसके नए आकाश-एनजी संस्करण में 80 किमी तक) की सीमा के साथ, यह 20 किमी तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को मार सकता है। तेज़ (मैक 2.5), मोबाइल, और राजेंद्र रडार से लैस जो एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक करता है, आकाश बहुमुखी है, जो जेट, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि क्रूज मिसाइलों का भी सामना कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का सुझाव है कि यह एक परमाणु हथियार ले जा सकता है, हालांकि इसका मुख्य काम हवाई रक्षा है। जैसे-जैसे ड्रोन सस्ते और आम होते जाएँगे, आकाश की भूमिका बढ़ेगी, लेकिन क्या यह चुपके से, कम उड़ान भरने वाले खतरों से निपट सकता है? यह एक चुनौती है जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए।
रूस में बना सिस्टम S-400 ट्रायम्फ भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, जिसे भारत तैनात कर रहा है। 400 किलोमीटर की रेंज, 30 किलोमीटर की ऊँचाई और 600 किलोमीटर दूर से खतरों को पहचानने की क्षमता के साथ, S-400 गेम-चेंजर है। यह 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और स्टील्थ जेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक 36 को निशाना बना सकता है। हालाँकि इसे परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन लंबी दूरी की ICBM को रोकना मुश्किल है, जिसकी सफलता दर कम है। S-400 की मिसाइलों का मिश्रण (40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज) एक स्तरित रक्षा बनाता है, लेकिन इसका रूसी मूल सवाल उठाता है। क्या भारत इसे घरेलू प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत कर सकता है? और अगर वैश्विक राजनीति स्पेयर पार्ट्स या अपग्रेड को सीमित करती है तो क्या होगा? भारत का आकाशीय किला टीमवर्क पर निर्भर करता है। PAD और AAD BMD कोर बनाते हैं, जबकि आकाश और S-400 व्यापक खतरों से निपटते हैं। प्रारंभिक चेतावनी रडार, सुरक्षित संचार नेटवर्क और कमांड सेंटर सभी को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे पल भर में निर्णय लेना सुनिश्चित होता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत की रक्षा को भेदना कठिन बनाता है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, AI-चालित झुंड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमारे सिस्टम का परीक्षण कर सकते हैं। स्वदेशी तकनीक के लिए DRDO का प्रयास आशाजनक है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। S-400, शक्तिशाली होने के साथ-साथ हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता ही अंतिम लक्ष्य है।
भारत की मिसाइल रक्षा शक्ति और नवाचार का प्रतीक है। यह दुश्मनों को डराता है, हमारे लोगों की रक्षा करता है और हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन आगे रहने का मतलब है निरंतर उन्नयन, अधिक परीक्षण और शायद अंतरिक्ष-आधारित सेंसर या लेजर सुरक्षा भी। एक राष्ट्र के रूप में, हमें अपने वैज्ञानिकों और सैनिकों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही कठिन सवाल भी पूछने चाहिए: क्या हम पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? क्या हम आज कल के खतरों का मुकाबला कर सकते हैं? भारत का आकाशीय किला मजबूत है, लेकिन केवल अथक प्रयास ही इसे अटूट बनाए रख सकते हैं।